शिक्षा के धर्मनिरपेक्षीकरण को लेकर विकसित होती बहस

‘हर गांव में एक दीपक जलाने वाला होता है – जिसे शिक्षक कहा जाता है ; और एक दीपक बुझाने वाला होता है – जिसे दुनिया पुजारी/पुरोहित के नाम से पुकारती है’
– विक्टर हयूगो ( 1802 – 1885 )
किसी दिन अगर आप को अपनी संतान के स्कूल से यह संदेश मिले तो आप क्या कहेंगे, जिसमें यह लिखा हो कि ‘ईश्वर, खुदा, नियंता, ‘पवित्र ग्रंथ’ आदि बातें आइंदा कक्षा में मना है !
क्या आप इस बात से सहमत होंगे या अपनी असहमति को प्रगट करने धड़ल्ले से स्कूल पहुंचेंगे ?
अमेरिका के प्राथमिक स्कूल की एक अध्यापिका ने ऐसे ही किया।
‘‘खुदा, ईसा मसीह और शैतान जैसे लब्ज कक्षा के बाहर ही रख दें’’।
पहली कक्षा के छात्रों के स्कूल के पहले ही दिन स्कूल अध्यापक द्वारा भेजे इस संदेश ने माता-पिताओं के एक हिस्से में जबरदस्त बेचैनी पैदा की थी। अपना प्रस्ताव रखने के पीछे अध्यापिका का एक सरल तर्क था। वह एक पब्लिक स्कूल की अध्यापक थी, जिसमें अलग अलग मजहबों और आस्थाओं से जुड़े बच्चे पढ़ने आते थे, और वह नहीं चाहती थीं कि ‘‘कोई बच्चा/बच्ची/माता-पिता इन लब्जों को सुन कर ही परेशान हो जाएं।’’ मुमकिन है उनके मुल्क में धर्म विशेष को लेकर या संप्रदाय विशेष को लेकर जो एकांगी किस्म की बातें फैलाई जा रही थी, समुदाय विशेष लांछन एक सहजबोध बन चुका था, वह चिंता भी उसके दिमाग में व्याप्त रही हो।
माता-पिताओं को भेजे अपने ख़त में उसने उन्हें यह भी सलाह दी थी कि आप जब चर्च/मंदिर/सिनेगॉग/मस्जिद – जहां पर भी जाते हों – जाएं तो उस दौरान अपनी संतान से इस मसले पर फुरसत से बात करें या मुफीद वक्त़ पर घर पर ही इस मसले पर चर्चा करें।’
बहरहाल, इसके बजाय कि यह बहस इस मसले पर केन्द्रित होती कि किस तरह ईश्वर की अवधारणा रफ़्ता रफ़्ता बाल मन पर आरोपित होती जाती है या किस तरह इस बहाने उसकी चिंतन प्रक्रिया को एक हद तक हम खुद कुंद करते जाते हैं , उल्टे मसला यह बना कि अध्यापक का यह सुझाव किस तरह ‘बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ पर आघात है। माता पिताओं के दबाव के मददेनज़र स्कूल प्रबंधन के लिए बहुत वक्त़ नहीं लगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।
गौर कर सकते हैं कि अपने सरोकारों के केन्द्र में बच्चों का कल्याण रखने वाले किसी भी शिक्षक को झेलने पड़ती इस उलझन में अनोखा कुछ भी नहीं है।
आप दक्षिण एशिया के इस हिस्से के स्कूलों में विज्ञान पढ़ा रहे किसी शिक्षक से बात कीजिए – भले ही वह निजी जीवन में आस्तिक हो मगर किसी दक्षिणपंथी जमात का हिमायती न हो, जो धर्म एवं समाजजीवन/राजनीति के घोल का प्रचार प्रसार करने में आमादा रहते हैं – और आप पाएंगे कि विज्ञान की आम बातें समझाने में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, तमाम वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद ग्रहण को लेकर आज भी अंधविश्वास कायम हैं, मध्यमवर्गीय परिवारों में भी इस पर बातें होती है, और ऐसे परिवार के बच्चे के लिए ग्रहण के पीछे के वैज्ञानिक तर्क को समझने में दिक्कतें झलनी पड़ती हैं ।
अग्रणी ब्रिटिश अख़बार ‘द गार्डियन’ ने एक अलग अन्दाज़ में ऐसी ही एक स्टोरी को सांझा किया था जिसमें अख़बार ने एक विज्ञान शिक्षक को कक्षा के अन्दर झेलने पड़ती दुविधा/कशमकश पर बात की थी। अध्यापक ने ‘‘उस चिन्ताजनक/उलझन भरी स्थिति को बयां किया था जब आप ऐसी बातें पढ़ा रहे होते हैं जो कुछ छात्रों के धार्मिक विश्वासों से बिल्कुल विपरीत होती हैं’’ या आप ‘‘ऐसे छात्रों से मिलते हैं … जिन्हें बचपन से इस बात पर विश्वास करना सीखाया गया होता है कि उनके विशिष्ट धर्म की पवित्र किताब में जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल सत्य बयां किया गया है।’’ अपनी निष्कर्षात्मक टिप्पणियों में अध्यापक ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर उचित विज्ञान शिक्षा प्रदान की जाए तो वह इन किशोरियों/किशोरों को ऐसी समझदारी से लैस करेंगे कि किस बात पर विश्वास किया जाए और किस पर न किया जाए, इसके बारे में वह अपने निर्णयों तक खुद पहुंच सकते हैं।
उदाहरण के लिए ‘द गॉड डिल्युजन’ नामक चर्चित किताब के लेखक रिचर्ड डॉकिन्स अपनी एक अन्य किताब ‘द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ: द इविडन्स फॉर इवोल्यूशन’ में अक्तूबर 2008 में 60 अध्यापकों के साथ चली बातचीत का हवाला देते हुए बताते हैं कि किस तरह एक अध्यापक ने बताया कि उनके छात्रा बाकायदा रोने लगे जब उन्हें बताया गया कि उन्हें इवोल्यूशन/क्रम विकास/उत्क्रांति पढ़ाया जाएगा। दूसरे अध्यापक ने बताया कि किस तरह विद्यार्थी ‘नहीं’ ‘नहीं’ करके चिल्लाने लगे जब उन्होंने इसके बारे में चर्चा शुरू की।..एक अन्य अध्यापक ने बताया कि किस तरह चर्च के लोग विद्यार्थियों को विशेष प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं ताकि उत्क्रांति पर चल रही मेरी कक्षा को नाकाम किया जा सके। / पेज 436,Blackswan /
अलग अलग पृष्ठभूमियाँ, अलग अलग अनुभव।
कहने के लिए यह चंद अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों के माध्यम से स्कूल की स्थिति के बारे में या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की चुनौतियों की बात की जा सकती है और यहभी जान सकते हैं कि महज शिक्षकविशेष तक बातें सीमित नहीं होती, राज्य की नीतियां भी उसके व्यवहार को लगातार प्रभावित करती हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए न पढ़ाया जाए इसके बारे में उसके आग्रहों से, सुझावों से प्रभावित होती हैं और इस बात से भी प्रभावित होती हैं कि स्कूल जिस समाज में बसा है, उस समाज की अपनी मानसिक-सांस्कृतिक -सामाजिक स्थिति क्या है, क्या वहां राजनीति से धर्म के अलगाव को लेकर, धर्म को किसी व्यक्तिविशेष के निजी मामले तक सीमित रखने और समाजजीवन में या राज्य के संचालन में उससे दूरी रखने के बारे में एक आम सहमति बनी है ? या क्या वह समाज इस कदर धार्मिकता में लिप्त है कि ‘पवित्रा धर्मग्रंथ’ से इतर लिखी अन्य बातें उसे बिल्कुल गंवारा नहीं ।
संयुक्त राज्य अमेरिका – दुनिया का सबसे ताकतवर जनतंत्र, जहां दुनिया के तमाम अच्छे अच्छेे विज्ञान के इन्स्टिटयूटस है, विज्ञान में आगे रिसर्च करने में इच्छुक युवाआं का अच्छा खासा हिस्सा वहां पहुंचने की हसरत रखता है – इसकी एक अलग मिसाल पेश करता है, फिलवक्त़ हम उससे सम्बधित पाठयक्रम के एक छोटे से ही पहलू की चर्चा करके आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वह भी बहुत कुछ कहता है।
पृथ्वी पर जीव की निर्मिति ?
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
Marie Curie ( 1867 – 1934 )
आदिम समय से मनुष्य को चंद सवाल परेशान करते रहे हैं ।
मसलन, समूचा ब्रहमांड किस तरह अस्तित्व में आया ?
इस पृथ्वी पर जीव कैसे निर्मित हुआ ? क्या वह सभी स्थानों पर निर्मित हुआ या किसी एक स्थान से शेष भाग में फैल गया ?
निश्चित तौर पर पहले ऐसे सवालों के जवाब पहले मिलना मुश्किल था, तो ऐसे समय में आदिम मानवी ने या मनुष्य ने अपने हिसाब से इसे समझा और बयान किया।
मिसाल के तौर पर अपनी आखरी किताब ‘ब्रीफ आनर्न्स टू द बिग क्वश्चन्स’ में महान भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग मध्य अफ्रीका की बोशोंगो ( Boshongo) जनजाति का जिक्र करते हैं। ( देखें, पेज 42, प्रकाशन John Murray, London ) इस जनजाति में यह मान्यता है कि
.””.सबसे पहले सिर्फ अंधेरा, पानी और महान खुदा बुम्बा था। एक दिन पेट दर्द से जबरदस्त कराहते हुए बुम्बा ने उलटी की और सूर्य को उगल दिया। सूर्य ने अपनी आग से कुछ पानी का सूखा दिया, और जमीन बच गयी। अभी भी दर्द झेल रहे बुम्बा ने फिर उलटी की और इस बार चंद्रमा,तारे और कुछ जानवरों – चीता, घड़ियाल, खरगोश और अंततः मनुष्य को उगला। “
19 वीं -20 वीं सदी में हमें इस दिशा में जवाब मिलने लगे।
इस संबंध में ब्रिटिश प्रकृतिवादी ( naturalist ) चार्ल्सस डार्विन ( 12 फरवरी 1809-19 अप्रैल 1882) ने नयी जमीन तोड़ी । प्राकृतिक चयन ( natural selection ) से विकास का डार्विन का सिद्धांत एक तरह से वह बुनियाद बना था जिसपर आधुनिक विकासवाद की वैचारिकी टिकी है । वर्ष 1853 में प्रकाशित डार्विन की बहुचर्चित किताब ‘आन द ओरिजिन आफ स्पेसीज़ ’ में इसे पहली दफा पेश किया गया था। वैज्ञानिक दायरों में तो उनकी बातें आसानी से फैलीं, उनकी बातों पर काम भी चलता रहा।
डार्विन का नाम तो दुनिया भर में फैल गया हो। लोगों ने अपनी अपनी पाठयपुस्तकों, किताबों में अनुरूप बदलाव किए और बहस जारी रही।
लेकिन रूढिवादी समाजों या धर्म की अधिक पकड़ रहनेवाले हिस्से में उसके स्वीकार में मुश्किलें पेश आयीं।लेकिन एक बेचैनी बनी रही।
इस बेचैनी की जड़ें दरअसल डार्विन के जीवननिर्मिति के गतिविज्ञान पर पड़नेवाली रौशनी से नहीं बल्कि उसके धर्मशास्त्राीय निहितार्थोंे में थीै। इसका मतलब यही था कि प्राचीन समय से जो मान्यता चली आ रही थी कि चाहे प्रकृति , ब्रहमांड, जीवन, मानवजीवन सभी किसी अलौकिक काम के जरिए वजूद में आए, इस पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना। धर्मग्रंथों की यह मान्यता कि जीवन के सभी रूप जो आज अस्तित्व में हैं वह हुबहू उसी तरह अस्तित्व में आए, किसी दैवी कार्रवाई के जरिए, उससे तौबा करना।
इस बेचैनी का प्रगटीकरण अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हुआ। अमेरिका में इसका प्रगटीकरण क्रिएशनिजम के विचार से हुआ, जोे एक तरह से उस धार्मिक विश्वास का पुर्नप्रगटीकरण था कि जीवन के सभी रूप जो आज अस्तित्व में हैं वह हुबहू उसी तरह अस्तित्व में आए किसी दैवी कार्रवाई के जरिए। अमेरिकी समाज के एक हिस्से में रूढिवादी ताकतों का इस कदर बोलबाला था कि सत्तर के दशक तक चंद राज्यों में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को पढ़ाना भी मना था। 1925 का एक किस्सा है कि तोे वहां एक अध्यापक जॉन थॉमस स्कोप्स इस बात कोे लेकर मुकदमा चला था कि उन्होंने अपनी कक्षा में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को पढ़ाया था।
इन दिनों ऐसे लोग जो डार्विन के विकासवाद से असहमत हैं, वह इंटलिजेन्ट डिज़ाइन – जो क्रिएशनिजम का ही थोड़ा सुधरा हुआ रूप है, उसकी बात करते हैं, जो ईश्वर की उपस्थिति को लेकर छदमवैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करता है।
आलम यह है कि आज भी औपचारिक तौर पर छह में से एक शिक्षक अभी भी डार्विन के विकासवाद के ‘सिद्धांत’ के बजाय ‘‘क्रिएशनिजम’ या उसकी कड़ी में आगे निकले ‘इंटेलिजेन्ट डिजाइन’ के सिद्धांत को पढ़ाता है। इतनाही नहीं पब्लिक हाईस्कूल के जीवशास्त्र के अध्यापकों का महज 67 फीसदी डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को मजबूती से पढ़ाता है कु छ लोग भले ही इंटलिजन्ट डिजाइन नहीं पढ़ाते हों , लेकिन वह डार्विन के सिद्धांत के प्रति थोड़ा ढुलमूल अवश्य दिखते हैं।
वैसे ताज़ा अध्ययन बताते हैं कि इस मामले में स्थिति थोड़ी सुधर रही है।
वैसे ऐसी बेचैनियां आप को बाकी मुल्कों में भी मिलती हैं, भले उन्होंने आधिकारिक तौर पर डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को कबूला हो।
भारत भी इसका अपवाद नहीं है। कुछ साल पहले का एक वाकया शायद इसी बात की ताईद करता है।
तत्कालीन मानव संसाधन राज्यमंत्री किसी सभा में बोलते हुए डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को खारिज किया था। उनका तर्क आसान था कि ‘‘डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत गलत है क्योंकि हमारे पुरखों ने इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया कि बंदर को आदमी में बदलते हुए उन्होंने देखा है।’’ अपनी यह निजी राय प्रगट करके ही वह खामोश नहीं हुए उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सिद्धांत के सिखाये जाने पर भी सवाल उठाए।
साफ था कि भारत के संविधान में वैज्ञानिक चिन्तन की जिस अवधारणा पर जोर दिया गया है, तथा जिसकी शपथ मंत्राीमहोदय ने खायी होगी, उसके साथ उनका यह बयान पूरी तरह बेतुका मालूम पड़ रहा था और इसी वजह से आम तौर पर सार्वजनिक बहसों से दूर रहनेवाले विज्ञान की विभिन्न संस्थाओं ने भी इस मसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने बयान में उन्होंने उनके वक्तव्य को सिरेसे खारिज किया। उन्होंने जोड़ा कि डार्विन का वैज्ञानिक सिद्धांत है और जिसके आधार पर ऐसी तमाम भविष्यवाणियां की गयी हैं जो प्रयोगों एवं अवलोकन के आधार पर सही साबित हुई हैं।’
पाकिस्तान कोे ही लें, जो दक्षिण एशिया में हमारा पड़ोसी है ; जहां पर भी विज्ञान शिक्षा के मामले में चीजें सुधरने के बजाय अधिक बिगड़ रही हैं।
उदाहरण के तौर पर जानी मानी पाकिस्तानी पत्रकार कामिला हयात ने कुछ समय पहले अपने आलेख में बताया था कि कितनी तेजी के साथ पाकिस्तानी शिक्षा संस्थानों में ‘काला जादू की अवधारणा, जिन्न और अन्य अदृश्य ताकतों को लेकर’ चर्चाएं लौट रही हैं। इस सन्दर्भ में उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा स्थापित एआईआर युनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैम्पस में आयोजित एक सेमिनार की चर्चा की थी जिसका फोकस जिन्नों पर तथा समाज में रहस्यमयी ;वबबनसजद्ध ताकतों की भूमिका पर था। बहुत अधिक प्रचारित इस सेमिनार की अध्यक्षता ‘अध्यात्मिक हदयविज्ञानी’ राजा जियाउल हक़ ने की थी। पत्रकार महोदया के मुताबिक यह कोई पहला ऐसा सेमिनार नहीं था, ऐसी संगोष्ठियां होती रहती हैं। जनरल जिया उल हक़ के जमाने से – जिन्होंने इस्लामिक विज्ञान की अवधारणा को लागू करने की कोशिश की थी – यह सिलसिला चल पड़ा है, जिस वक्त़ ऐसे ‘सिद्धांत’ भी प्रमोट हुए थे कि जिन्नों से हासिल उर्जा को हम इंधन की कमी को दूर करने तथा अन्य मुददों को सुलझाने में कर सकते हैं।
उनके इस आलेख ने मशहूर पाकिस्तानी भौतिकीविद एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता परवेज हुदभॉय के अन्य आलेख की याद ताज़ा की थी, जिसमें उन्होंने इन्हीं जनाब के कुछ साल पहले सम्पन्न इस्लामाबाद के अन्य व्याख्यान पर – जिसका फोकस जिन्नों पर तथा समाज में रहस्यमयी ;वबबनसजद्ध ताकतों की भूमिका पर – चर्चा की थी और बताया था कि ऐसे आयोजन अब लोकप्रिय हो चले हैं। पैरानार्मल ज्ञान के विशेषज्ञ आए दिन वहां के स्कूलों-कालेजों में पहुंचते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कराची के मशहूर इन्स्टिटयूट फॉर बिजनेस मैनेजमेण्ट ने ‘मनुष्य के आखरी पल’ विषय पर बोलने के लिए ऐसे ही किसी शख्स को बुलाया था। उन्होंने यह भी बताया था कि पखतुनवा प्रांत में पाठ्यक्रम के लिए तैयार जीव-विज्ञान की किताब डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर देती है।
चाहे अमेरिका हो , चाहे पाकिस्तान या भारत – हम पाते हैं कि विज्ञान ने जिस सिद्धांत को अधिक स्वीकारणीय बनाया है , उसे पूर्णतः स्वीकार में लोगों के एक हिस्से को – भले कहीं कम हों या कहीं ज्यादा हो – मुश्किलें पेश आ रही है क्योंकि कही न कहीं ईश्वर की, गॉड की या खुदा की छाया पाठयक्रम पर पड़ी हुई हैं, जो उन्हें उन बातों के पूर्ण स्वीकार में बाधित करता है।
छात्र के लिए अधिक मुश्किल होता होगा वह विज्ञान पढ़ भी रहा है और साथ साथ उससे जुड़ी छदम वैज्ञानिक व्याख्या को भी पढ़ रहा है , जो उसे अधिक उलझा देता है।
दूसरा तरीका हो सकता है कि धर्म की चर्चाओं को, ईश्वर के बारे में गुफ्तगू को पिछले दरवाजे से भी प्रवेश देने का हो सकता है।
भारत इसकी एक नायाब मिसाल पेश करता है, जिसने अपनी आज़ादी के बाद साफ साफ ऐलान किया था कि ‘राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
धार्मिक शिक्षा पिछले दरवाजे से
“राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ..खंड /1/ की बात ऐसी शिक्षा संस्था में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था को धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। संविधान की धारा 28/1/
धारा की अगली कड़ी कहती है:
… राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है।“
कहा जा सकता है कि 40 के दशक के उत्तरार्द्ध में जब दक्षिण एशिया का यह हिस्सा धार्मिक उन्माद से फैली हिंसा से उबरने की कोशिश में मुब्तिला था, उन दिनों स्वाधीन भारत के संविधान निर्माताओं ने बेहद दूरंदेशी का परिचय दिया। उस घड़ी में ही जब आपसी खूंरेजी उरूज पर थी, उनके सामने यह बिल्कुल साफ था कि अगर मुल्क को प्रगति की राह पर ले जाना है तो बेहतर है कि एक नयी जमीन तोड़ी जाए, स्कूल/शिक्षा संस्थान – जिनका बुनियादी मकसद बच्चों/विद्यार्थियों के दिमाग को खोलना है और उन्हें बेकार की चीज़ें ठूंसे जाने का गोदाम नहीं बनाना है – धार्मिक शिक्षा से दूर रखे जाएं।
यहां इस बात को रेखांकित करना आवश्यक है कि धार्मिक शिक्षा का यह सीमित अर्थ है। वह इस बात को सम्प्रेषित करता है कि रस्मों रिवाजों की शिक्षा, पूजा के तरीके, आचार या रस्मों को शैक्षिक संस्थानों के परिसरों में अनुमति नहीं दी जा सकेगी जिन्हें राज्य से समूचे फंड मिलते हों।
संविधान की धारा 28 /1/ महज इस मामले में अपवाद करती है कि कि अगर कोई शिक्षा संस्थान किसी ट्रस्ट के तहत या किसी एंडोमेंट के तहत स्थापित किया गया हो, जहां पर धार्मिक शिक्षा देना जरूरी होता हो, तो वहां चाहे तो प्रबंधन इस मामले में फैसला ले सकता है। धारा 28 /2/
वैसे जैसे जैसे आज़ादी के 75 वीं सालगिरह को लेकर समारोहों, ऐलानों की बाढ़ आ गयी है, हम खुद देख रहे हैं कि ब्रिटिशों की गुलामी के दौरान चले राजनीतिक-आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक मुक्ति संघर्षों में हासिल अहम सबकों को कितनी आसानी से भुलाया जा सकता है, किस तरह बेहद आसानी के साथ धार्मिक शिक्षा के लिए दरवाजे सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में खोले जा सकते हैं !
क्या इसकी अहम वजह मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों, ताकतों के हाथों में पहुंचना है , जिन्होंने उस ऐतिहासिक संघर्ष की विरासत को कभी भी अपना नहीं कहा ? इस बात की पड़ताल जरूरी है।
इस मामले में सबसे ताज़ा मसला मध्य प्रदेश में सामने आया है जब बीए के दर्शन के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रामचरितमानस के दर्शन को एक वैकल्पिक विषय के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, उसके साथ ही वह ‘रामसेतु की चमत्कारी इंजिनीयरिंग’ के पाठ भी पढ़ेंगे और ‘राम राज्य के आदर्शों’ पर भी सबक ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि अपने लिए किसी असुविधा से बचने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह कदम किसी विशिष्ट धर्म के बारे में नहीं है और उसमें ‘विज्ञान, संस्कृति , साहित्य और श्रृंगार ’/ भारतीय क्लासिकल कला रूपों में प्रेम और सौंदर्य की अवधारणा/ पर भी बात होगी।
इस संदर्भ में एक बात ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि कोविड महामारी के दौरान लायी गयी नयी शिक्षा नीति ने ऐसे कदमों को उठाने को और सहूलियत प्रदान की है क्योंकि उसके तहत प्रस्तुत ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ में ऐसे विषयों को शामिल करना आसान है।
महज कुछ माह पहले मुख्यधारा की मीडिया में इसके बारे में रिपोर्ट छपी थीं कि शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त ढंग से संचालित एनआईओएस अर्थात नेशनल इन्स्टिटयूट आफ ओपन लर्निंग ने मदरसों में गीता और रामायण को ले जाना तय किया है।राजस्थान की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने किस तरह अपने कार्यकाल में स्कूलों में विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संत महात्माओं को बुलाना तय किया था और किस तरह उसे बुद्धिजीवियों तथा नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के प्रबल विरोध के चलते उस फैसले को वापस लेना पड़ा था, यह बात भी सर्वविदित है।
अगर हम मध्यप्रदेश के कालेजों में वैकल्पिक पाठयक्रम के तौर पर रामचरितमानस के प्रस्ताव पर नए सिरेसे लौटें, तो पता चलता है कि उसे योग और ध्यानधारणा के साथ ‘बच्चों के सर्वांगीण विकास’ के लिए पढ़ाया जाएगा। दरअसल सरकार को यह लगता है कि इसके चलते उनके अंदर ‘मानवीय रूख के विकास’ में प्रगति हो सकेगी और विद्यार्थियों में ‘जीवनमूल्य’ भी संस्कारित किए जा सकेंगे।
‘पवित्र ग्रंथ’ और अन्य
क्या धार्मिक किताबों से लोगों के नैतिक आचरण में विकास होता है या वह अधिक संकीर्ण होे जातेे हैं, फिलवक्त़ हम भले ही इस बहस में न जाएं कि लेकिन एक बात पर हमें सोचना ही पड़ेगा कि विभिन्न धर्मों की ‘पवित्र किताबों में अन्य के लिए क्या कहा गया है ?
दरअसल अगर हम बारीकी से देखें तो विभिन्न धर्मों के इन ग्रंथों में हमें ऐसी तमाम बातें मिल सकती हैं जो ‘अन्यधर्मीय’ के लिए असमावेशी प्रतीत होती हों यहां तक कि समाज की सोपानक्रम नुमा संरचना को वैधता प्रदान करती हों या समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा का आवाहन करती दिखती हैं। ऐसी किताबें या उनके अंश पाठ्यक्रम में पहुंच जाए तो वह किस किस्म के वातावरण का निर्माण करेंगे ? और इस स्थिति में यह सवाल उठना लाजिमी हो जाता है कि ऐसे पाठों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्यों स्थान दिया जाए ?
हमें यह भी सोचना चाहिए कि पाठयक्रम में अगर किसी धर्म विशेष की बातें या उससे जुड़ी किताबें, ग्रंथ शामिल किए जाएं तो इसका बेहद विपरीत असर उन विद्यार्थियों पर पड़ सकता है जो अज्ञेयवादी हों या निरीश्वरवादी हों या दूसरे धर्म, संप्रदाय से ताल्लुक रखते हों। इस संदर्भ में खुद नेशनल कौन्सिल फार एजुकेशनल रिसर्च एण्ड टेनिंग का अध्ययन गौरतलब है, जिसके द्वारा तैयार किए गए मैन्युअल का फोकस लगभग इसी बात पर है कि स्कूल असेम्ब्ली में होनेवाली प्रार्थनाएं और इनकी दीवारों पर चस्पां किए गए देवी देवताओं की तस्वीरें किस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में पार्थक्य की भावना पैदा करते हैं। उसने यह भी सुझाव दिया है कि स्कूलों के अन्दर धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े त्यौहारों को प्रोत्साहित किया जाए, स्कूल के अन्दर धार्मिक आयोजनों में ऐसे बच्चों के साथ अधिक संवेदनशीलता के साथ पेश आया जाए।
इस मसले की पड़ताल करते हुए हम संविधाननिमाण के दौरान चली बहसों पर भी गौर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्वाधीनता के संग्राम की अगुआई करनेवाले उन दूरंदेशी रहनुमाओं ने – जिनमें से अधिकतर आस्तिक ही थे – इस बात का विरोध किया था कि संविधान में ‘ईश्वर के नाम’ को अनिवार्य किया जाए। :
“..17 अक्तूबर 1949 को एच वी कामथ ने संविधान के प्राक्कथन में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। उनका सुझाव था कि ‘वी द पीपुल आफ इंडिया अर्थात ‘हम भारत के लोग’ के पहले ‘ईश्वर के नाम’ अर्थात ‘इन द नेम आफ गॉड’ का उल्लेख किया जाए। मालूम हो कि संविधान सभा में इस मसले पर तीखी बहस चली, सदस्यों ने इस संशोधन के खिलाफ अपनी भावना प्रगट की और अंततः उसे खारिज किया। एक सदस्य पटटम ए थाणु पिल्लेई ने कहा कि इसका मतलब आस्था को अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने जोड़ा ‘‘ वह आस्था की स्वतंत्राता के बुनियादी अधिकार को प्रभावित करता है। संविधान के मुताबिक किसी व्यक्ति को ईश्वर पर आस्था रखने या नहीं रखने का अधिकार है।’’एक अन्य सदस्य हदयनाथ कुंजरू ने कहा कि प्राक्कथन में ईश्वर का नामोल्लेख करना एक तरह से ‘‘एक संकीर्ण, संकुचित भावना को उजागर करता है जो संविधान की मूल स्पिरिट के प्रतिकूल है।’’
यह भी विचारणीय है कि क्या नैतिक शिक्षा के नाम पर कोई शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों पर धार्मिक शिक्षा लेने से मजबूर कर सकता है, जैसी बात कुछ रूढिवादी कर सकते हैं कि हम फलां धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाये जाने की हिमायत इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे अधिक नैतिक बनें।
मसविदा कमेटी ने अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रखते हुए यह कहा था कि विद्यार्थी पर ऐसा कोई भी दबाव बनाना संविधान की धारा 19 का उल्लंघन होगा क्योंकि ‘‘सभी नागरिकों को बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ’’ इतनाही नहीं इस तरह का कोई भी आरोपण धारा 25 /1/ का भी उल्लंघन होगा“ जिसके मुताबिक ‘‘इस हिस्से की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के मसले को देखते हुए , सभी लोगों को जमीर की पूरी आज़ादी होगी और धर्मविशेष को मुक्त रूप में प्रसारित करनेे, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्राता होगी।’ (“Subject to public order, moraility and health and to the other provisions of this Part, all person are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.”)
आज भले ही इस इतिहास को भुला दिया जा रहा हो लेकिन यह बात इतिहास में दर्ज है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण /साइंटिफिक टेम्पर/ के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्राी रहे जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले से सक्रिय थे। दरअसल संविधान के बुनियादी कर्तव्यों में वैज्ञानिक चिन्तन को शामिल करने के पीछे उन्हीं का अहम योगदान था। आजादी के संघर्ष के दौरान लिखी उनकी बहुचर्चित किताब ‘भारत एक खोज’ में उन्होंने कहा था:
: ‘आज के समय में सभी देशों और लोगों के लिए विज्ञान को प्रयोग में लाना अनिवार्य और अपरिहार्य है. लेकिन एक चीज विज्ञान के प्रयोग में लाने से भी ज्यादा जरूरी है और वह है वैज्ञानिक विधि जो कि साहसिक है लेकिन बेहद जरूरी भी है और जिससे वैज्ञानिक दृद्रष्टिकोण पनपता है यानी सत्य की खोज और नया ज्ञान, बिना जांचे-परखे किसी भी चीज को न मानने की हिम्मत, नए प्रमाणों के आधार पर पुराने नतीजों में बदलाव करने की क्षमता, पहले से सोच लिए गए सिद्धांत की बजाय, प्रेक्षित तथ्यों पर भरोसा करना, मस्तिष्क को एक अनुशासित दिशा में मोड़ना- यह सब नितांत आवश्यक है. केवल इसलिए नहीं कि इससे विज्ञान का इस्तेमाल होने लगेगा, लेकिन स्वयं जीवन के लिए और इसकी बेशुमार उलझनों को सुलझाने के लिए भी…..वैज्ञानिक द्र्रष्टिकोण मानव को वह मार्ग दिखाता है, जिस पर उसे अपनी जीवन-यात्रा करनी चाहिए. यह दृद्रष्टिकोण एक ऐसे व्यक्ति के लिए है, जो बंधन-मुक्त है, स्वतंत्र है.’
जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि रफ़्ता रफ़्ता रफता धार्मिक शिक्षा के लिए रास्ता सुगम किया जा रहा है, हमें यह भी याद रखना चाहिए और हमें सत्ताधारियों को ही नहीं आम जनता को भी बताना चाहिए कि संविधान की एक अहम धारा है जो नागरिकों के बुनियादी कर्तव्यों की बात करती है, जिसमें ‘‘वैज्ञानिक चिंतन, मानवता और जांच पड़ताल की भावना और सुधार’’ की बात शामिल है। धारा 51 ए बुनियादी कर्तव्यों के बारे में)। कहने का तात्पर्य यह कि जैसे जैसे धार्मिक शिक्षा आम होती जाएगी, वह वैज्ञानिक चिंतन के विकास को बाधित करेगी। शायद उन्हें यह भी बताना होगा कि धार्मिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना समानान्तर धाराएं हैं और आपस में नहीं मिलतीं।
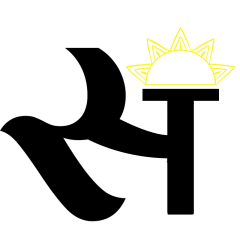
I hold opposite view. My father was head master of the school, where I studied. He used to invite religious leaders of several type and we used to enjoy those talks. My father was a Gandhian. We learned important lessons from Srimad Bhagawat Gita and Bible. In our town Quran was not available. My father also used to make fun of several aspect of mythical stories. I learned how to take religion lightly and also seriously.
Class rooms are to enrich ourselves. God is a very important issue that address our very existence on this earth. Why are we here? What is the purpose of the creation? These are powerful questions, we can not avoid them, no matter how much we try. I know, there is no answer to these questions, but they are questions and we ponder on them. Wise man of all time pondered on them. And, they took the form of religion. Selfish thugs (in all ages), want to make a living by highlighting the irrelevant aspect of the work of those masters. But, great wise masters appeared and dominated. Sri Ramakrishna, Swamy Sivananda are some examples, I know. There may be many more around the world.
I do not much know, what others advise on religion, but my opinion is take it hard on. Talk about it more. Actually, I look for people who are willing to talk for or against religions. Last week, we had a party in our home, when I showed a Holy Quran that got from Istanbul, many got surprised. I just asked them, if I call Sri Jaganath Mahabrabhu as Allha, will He scold me? Will He not respond to my call? They said, He will surely respond. So, where is the problem. They said, you are wise, but not others. Why not others? Let us talk. Let us all be wise and talk what ancient wise man talked. Let us enjoy what Goswami Tulasidas said. Yes, he said some things not good about women and Sudra, but he said many good things on many aspects. Some total, he was much wiser than many of us.
My opinion: let us talk about more about God in class room. Bring your religion – Srimad Bhagawat Gita, Bible, Quran Sarif or Guru Grantha Sahib. These are treasures, I think. When we stop talking religion, Thugs will talk outside the classroom and people will listen. That is the problem, when our classrooms are devoid of God.
पसंद करेंपसंद करें
Thanks for the detailed comment about the piece
-It is really exciting to know about your personal experience where there use to be discussion and debates – sometimes critical as well – about various religions. Looking at the times you had your schooling or the ambiance which existed then your experience cannot be considered an exception, there were many such schools / teachers who could be accommodate such diversity of experiences / experiments.
My own own experience was the exact opposite despite the fact that the school was not run by any religious organisation or a self proclaimed cultural organisation
– Agree that class room is definitely a place to enrich ourselves and raise all sorts of questions – right from our endless curiosities to the meaning of life questions – and not necessarily reaching any conclusion but keep the debate going and ideally we should definitely strive towards them.
I have two broad queries / concerns towards any such proposal.
– With the growing deterioration of any debate in our society and around, with a greater emphasis on homogeneity, unity, equating democracy with no voice for minority view, one has serious doubts whether such discussions / debates are possible today especially regarding various religions within the confines of the classroom
A related query is religion is not just good thoughts by the wise wo/men of the faith, every such worldview has quite a few negative things to say about others’. One can cite examples from scriptures which deny humanity even to a section of its own followers or ask its followers to ”lynch’ or ‘eliminate’ others.
One cannot avoid discussion around such contentious topics once the theme opens up and definitely the consequences can be easily foreseen.
– Secondly, one feels that indoctrination in particular faith – which starts from our infancy / childhood – in very many ways, and proceeds further the way you choose your school, can have a long term impact on one’s inquisitiveness, which could be seen as a first step towards real learning
When a parent asks the child to close eyes before an idol because it is Supreme, it inadvertently or so inhibits is blossoming slowly
पसंद करेंपसंद करें